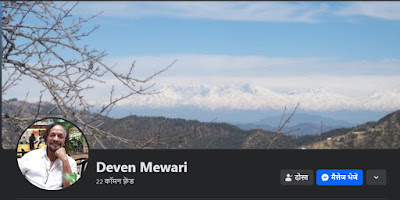आरामकुर्सी से-
उस जमाने के शब्दचित्र, जब मोबाइल-इण्टरनेट नहीं हुआ करते थे...

Saturday, 24 February 2024
"अमीन सायानी...बचपन की आवाज़ का खामोश होना"- राजेश ज्वेल
"चवन्नी पर कॉमिक्स"- दीपक कुमार सिंह
"ओ हमारे प्यारे रेडियो" - देवेन मेवारी
"मकर संक्रान्ति" - विजया एस. कुमार
"याद किया दिल ने कहां हो तुम" - ध्रुव गुप्त
"जाड़ों के वे दिन" —राम अयोध्या सिंह
क्या वे भी जाड़े के दिन थे। चाहकर भी मैं अपने बचपन के दिनों को भूला नहीं पाता। खाने के मामले में जाड़े का मौसम वास्तव में मौसम का बादशाह था। गर्म या ऊनी कपड़े भले ही पहनने को नहीं थे, पर खाने और खेलने से ही शरीर में इतनी गर्मी रहती थी कि कपड़े की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। सुबह उठते ही शौच के बाद बरामदे में बोरसी के पास या धूप में बैठकर बासी भात और चने-सरसों की साग और साथ में आम के अचार का तो कहना ही क्या? एकदम लसारके खाइये, कोई हर्ज नहीं। इसके बाद दो घंटे तक गाँव की गलियों, खलिहान या दालान पर साथियों के संग खेलिए। पता ही नहीं चलता था कि पेट कब खाली हो गया? इसके बाद फिर से स्कूल जाने के पहले गरमा-गरम भोजन का इंतजार। भाप निकलता भात, मटर की हींग से तड़का लगी दाल, आलू-बैगन और मटर की तरकारी और कभी जल्दबाजी में सिर्फ भात और तरकारी खाकर ही झोला उठाकर दो किलोमीटर दूर संदेश स्कूल में पढ़ाई के लिए रवाना।
स्कूल से लौटकर फिर वही दिन वाला खाना, और गांव में खेलकूद, मारपीट और दौड़ा-दौड़ी। कबड्डी, बुढ़िया कबड्डी, चिक्का, बांड़ी चिक्का, लुकाछिपी या कभी रबर की गेंद का खेल। खेलते-खेलते ही पुनः भूख का एहसास होने लगता था। यूँ समझिये कि खाना और खेलना ही हमारा प्यारा शगल था। पढ़ाई ऊपर-झापड़ ही होती थी, और उतनी ही होती थी, जिससे स्कूल में माट्साब से पीटें नहीं, और परीक्षा में पास हो जायें। अंधेरा घिरते ही पेट भोजन के लिए कुलबुलाने लगता था। तब हमारे गाँव में सुबह, दिन और रात सिर्फ भात ही लोग खाते थे, खासकर जाड़े के दिनों में। रात में फिर वही भात, मटर की दाल और आलू, बैगन, मटर और सेम की तरकारी। कभी-कभार भात और तरकारी से भी काम चल जाता था। मुझे तो भात और तरकारी आज भी अच्छा लगता है। अगर घर में चने की साग है, तो शायद ही तरकारी की जरूरत पड़ती थी। चने की साग में हरी मिर्च, हरे लहसुन की पत्तियाँ और सरसों का तेल या अचार का मसाला मिलाया जाता था। इसके बाद कौन कहाँ तरकारी खोजता था? भात और साग लसारकर खाइये। कभी-कभी कोबी (गोभी) की तरकारी भी मिलती थी, पर ऐसा कभी-कभी ही होता था। हाँ, कोहड़ा, कद्दू और नेनुआ की तरकारी जरूर मिलती थी। इसके पौधे हर कोई अपने घर के छप्पर या आलान पर चढ़ा देता था। कच्चे कोहड़े की तरकारी ही मुझे अच्छी लगती है। पक्के कोहड़े की तरकारी मैं आज भी पसंद नहीं करता हूँ। कद्दू और नेनुआ की तरकारी कैसे भी करके बनाई जाये, मुझे पसंद है। इनके साथ मैं भात सानकर आराम से खाता था। अगर इसके साथ मट्ठा मिल जाये तो फिर बात ही क्या? कोहड़े के पत्ते की साग भी मैं बड़े चाव से खाता था। अब तो यह मिलता ही नहीं।
पर, जाड़े में भात, चने की साग, दाल, तरकारी, चोखा, अचार और दही या मट्ठे के अलावा चूड़ा और लाई भी अफरात में मिलता था। चूड़ा तो कातिक माह से ही शुरू हो जाता था, जब कतिका धान पकने पर आता था। पकने के पहले ही उसे खेतों से काट लिया जाता था, और घर की औरतें आंगन में ही पीटकर धान निकालती और फिर ओखल में मूसल से कूटकर चूड़ा बनाती थीं। हरे धान की सौंधी महक वाले चूड़े की बात ही कुछ और थी। कितना भी खाइये, पेट तो भर जाता था, पर मन नहीं भरता था। इसके अलावा लाई (चूड़ा, चावल, धान, बाजरा, ज्वार) की भी भरमार होती थी। कौन कितना खा रहा है, इसकी कोई गिनती नहीं थी। वैसे भी यह भोजन में गिना भी नहीं जाता था। इसे लोग ऊपरवार मानते थे। चूड़ा और लाई के अलावा सोंठ और मेथी के लड्डू भी बनते थे। इन सब कामों में मेरी आजी गाँव में चुनिंदा थी। लोग उसे अपने घर खुशामद करके बुलाते थे। जाड़े भर में हर कोई इतना जरूर खाता था कि उसके शरीर के ऊपर चर्बी दिखाई पड़ने लगे। यहाँ तक कि पशुओं का शरीर भी मोटा-ताजा होकर चमकने लगता था। पर, इन सबसे ऊपर था मटर और फिर चने का होरहा, जिसे बधार में किशोर वय के लड़के और नवजवान तैयार करते थे, और जो बच जाता था, वह घर की औरतों के लिए होता था। होरहे के साथ आजवाईन मिला नमक, हरी मिर्च, अदरक और कभी-कभी नींबू की नीमकी भी हाथ में लोग खाते थे। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि गांववाले भी खुद इनके लिए तरस रहे हैं। चने और मटर की खेती गाँव से खत्म हो गई है। मौसम में कभी मिल जाये, तो इसे सौभाग्य ही लोग समझते हैं।
***
"मेले में भोंपा" —चंचल
गाँव में कातिक अगहन, ये दो महीने मेला-ठेला के होते आये हैं। धान की फ़सल कट कर सटकने के लिये समथिया जाती रही। इसी में मेला का खेल शुरू होता था। आँखन-देखी और आप-बीती बताऊँगा, तो कल और आज के बीच आया बदलाव साफ़ साफ़ समझा जा सकेगा। उस जमाने में कोई भी काम “तुरतिहा“ नहीं था, आहिस्ता-आहिस्ता अपने उफ़ान पर पहुँचता था। ज़िंदगी हो, उत्सव हो, उत्पादन हो या बात बतकही हो, या फिर प्यार-व्यार ही क्यों न हो— सब आहिस्ता-आहिस्ता ही शुरू होता रहा, आज की तरह तुरतिया संस्कृति नहीं आयी थी।
आज विजय दशमी है। इस दिन को कुछ ख़ास ख़ास स्थानों पर ही विजय दशमी का मेला लगता रहा। इस तारीख़ का इंतज़ार गाँव हफ़्ते भर पहले से शुरू कर देता था। नये कपड़े बनते, पुराने “रेहिआये“ जाते ।
-रेहिआये? ऐसा अंग्रेज़ी मत ठेलो कि पल्ले ही ना पड़े!
-इसे सीधा कर लो, अंग्रेज़ी बोलूँ, तो तुरत समझ जाओगे। यह जो अंग्रेज़ी है न, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ती, फिर भी समझ में आ जाती है, क्यों कि तुम अंग्रेज़ी का पल्लू थामे दौड़ रहे हो, कितना भी लतियाये जाओ, छोड़ोगे नहीं अंग्रेज़ी, क्योंकि अब तक अंग्रेज़ी भाषा थी, आज बाज़ार की सामग्री है और यह सामग्री तुम्हारे ज़रूरी ज़रूरियात है। मसलन टूथ पेस्ट, ब्रश, कोल्ड ड्रिंक, कुरमुरे, बिस्कुट, कहाँ तक गिनायें। वो भाषा, जो किसी सामग्री के साथ दासी के रूप में आती है, उसे पढ़ना या समझाना नहीं पड़ता, अगला कदम बढ़ाने के लिये उसे गेल में डाल लेना पड़ता है। अब देखो- अस्सी के फेटे में खड़े लम्मरदार, जो आज भी आदिम युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुतिया छाप मारकीन की बँहकटी बंडी और लट्ठे की मोटी मटमैली धोती घुटने के ऊपर लपेटे, केवल लिबास से ही पीछे नहीं रह गये हैं, खानपान, रहने का सलीका भी वही पुराना ही है। और तो और- विकास (?) की हर तकनीक और कारख़ाने के छली उत्पाद के मुखर विरोधी भी हैं। घर में चाय-बिस्कुट, कप-प्लेट तक वर्जित है, आज भी वे जल जलपान में चना-चबैना और गुड़ से मेहमानों की आवभगत करते हैं, लेकिन कल की बात है, लबे सड़क उनकी आमद ने गाँव को चौंका दिया। भूरे रंग का चड्ढा, जिसके दोनों जाँघों पर तीन-तीन इंच की तीन-तीन लाल की धारी छपी हुई, ऊपर नारंगी रंग की टी-शर्ट, सीने पर अंग्रेज़ी में “रब मी नाट“ की मोटी काली लिखावट में हौले-हौले चले आ रहे हैं, कंधे पर तीन-चार साल का एक लड़का चीख़ता-चिल्लाता लम्मरदार का सिर पीटता बैठा है। गाँव कनमाना कर खड़ा हो गया। उमर दरजी, जो लछमीना के ब्लाउज़ का नाप ले रहा था, लम्मरदार को इस भेस में देख कर चौंक गया, फ़ीता लिये दिये दलान से बाहर आ गया,
-लम्मरदार, तू?
-हम ही अही, बोल।
उमर कुछ बोलते, उसके पहले कंधे पर बैठा लड़का सप्तम में आ गया और लगा जोर-जोर से हाथ पाँव चलाने। उमर ने दूसरा सवाल दागा,
-ई लड़िका के अहय?
-नाति अहय, तुन्नी क छोटका लड़िका, सुबहय से “टोन-टी“, “टोन-टी“ किए जात बा।
इस वाक़ये का अंत हुआ राम लाल गुप्ता की दुकान पर जाकर, जब लड़का लम्मरदार के कंधे से उतर कर दुकान में घुसा और अपनी पसंद का बिस्कुट लेकर बाहर निकला, तब तक लम्मरदार अंग्रेज़ी भाषा का एक शब्द कंठस्थ कर चुके थे।
गाँव में केवल शहरी उत्पाद और उस पर चिपकी भाषा ही नहीं आ रही, साथ-ही-साथ गाँव अपना उत्पाद तो ख़त्म कर ही रहा है, अपनी शब्द-सम्पदा को भी गँवा रहा है। “रेहिआना“ कपड़ा धोने की एक क्रिया रही, जो मुफ़्त सुलभ एक नैसर्गिक उत्पाद था/है। रेह मिट्टी का एक प्रकार है, जो छारीय होती है। साबुन, डिजर्जेंट, लिक्विड आदि आने के पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कपड़े की धुलाई इन्हीं प्राकृतिक उत्पादनों से ही होती थी। कपड़े की और बाल की सफ़ाई के लिये वनस्पतियाँ का बहुतायत से प्रयोग होता। इनमे “रीठा,“ तिल की पत्तियाँ, घृतकुमारी (एलोबेरा) प्रमुख और सर्वसुलभ हैं। गाँव की सामूहिक विनमय प्रथा, समाज की हर समस्या की खोज पर ज़िंदा और स्वावलंबी रहा। कपड़े की सफ़ाई भी उनमें एक था और इस काम को अंजाम देने वाले धोबी थे। कपड़े ले जाते रहे और बकरी की लेड़ी के साथ सान कर कपड़ों की भीनने के लिये रख देते। तीन चार दिन बाद इन कपड़ों की धुलाई करते। इसे रेहियाना कहते हैं। यह बात बता रहा हूँ, जब भारत टटकै आज़ाद हुआ था, दुनिया द्वितीय विश्वयुद्ध से गुजर कर टूट चुकी थी, उसी मुहाने पर भारत को तबाह करके अंग्रेज यहाँ से विदा हुए थे। हर तरह की क़िल्लत से भारत गुजर रहा था, सिवाय एक “आंतरिक ख़ुशहाली“ से, क्योंकि भारत गाँवों का देश है और गाँव की सबसे बड़ी पूँजी है- उसकी सहनशक्ति और अभाव में स्वप्निल भविष्य की अभिलाषा। उस जमाने में “मेला“ गाँव का उत्सव पर्व होता था। हमारे इलाक़े में तीन-चार बड़े मेले लगते, बाक़ी इलाक़ायी। हम बच्चों को “इत्ती दूर पैदल कहाँ जाओगे, गाँव भी तो वही मेला लगेगा, जम के देखा जायगा” -बोल कर फुसलाया जाता और हम मान भी जाते ।
उन दिनों हमारे गाँव के बिलकुल नज़दीक एक गाँव है- क़ोल, हम बच्चे सज-धज कर “कोल क मेला“ देखने की तैयारी करते। बालों में सरसों का तेल, आँख में काजर चभोरे चलते मेला देखने। गाँव के मानिंद लोग इस मेले के आयोजन में भरपूर सहयोग करते। हमारे जमाने में इन आयोजकों में चरित्तर तिवारी, नन्हकू सिंह, शोभा सिंह वग़ैरह बड़ी मुस्तैदी से लगे रहते। प्लास्टिक तब तक गाँव में नहीं आया था। बच्चों के खिलौने भी गाँव के उत्पाद से तैयार किए जाते। उस जमाने में ताड़ के पत्ते से झुनझुना और भोंपा बिकता था, क़ीमत एक “छेदहवा पैसा“ और इतने का ही भोंपा मिलता। मेले में बमुश्किल से तीन या चार तरह की मिठाई बिकाती थी- गट्टा, दो तरह की जलेबी (चिनीअहिया और चोटहिया) और एक मशहूर और सस्ती मिठाई होती थी, उसे कंकड़हिया मिठाई बोलते थे, चीनी गला कर छोटे छोटे साँचे में ढाल कर बनायी जाती। इसमें हाथी, ऊँट, मछली वग़ैरह के साँचे होते। अंत में रावण जलता उसके पेट में रखा पटाखा फूटता और यही पटाखा बताता की अब मेला विसर्जित हो गया। दुअन्नी में मेले का आनद बटोरते हम बच्चे भोंपा बजाते घर लौटते।
अब सब बदल गया है। सिक्के तक।
***
"अमीन सायानी...बचपन की आवाज़ का खामोश होना"- राजेश ज्वेल
उज्जैन के पटनी बाजार में तोतला भवन की पहली मंजिल का मकान और गोदरेज की अलमारी के ऊपर रखा ट्रांजिस्टर... हर बुधवार की सुबह से ही ट्रांजिस्टर...

-
उज्जैन के पटनी बाजार में तोतला भवन की पहली मंजिल का मकान और गोदरेज की अलमारी के ऊपर रखा ट्रांजिस्टर... हर बुधवार की सुबह से ही ट्रांजिस्टर...
-
बात थोड़ी संजीदा है। भारतीय रेल से हम सबका थोड़ा-बहुत लगाव है। कुछ भावनात्मक रिश्ता जैसा भी है। बचपन में हम सब कतारबद ्ध होकर रेल का ख...
-
स्कूल जाने के लिए घर के पिछवाड़े के खेत की मेड़ से जाना होता। बना में सबसे पहले बरगद का विशाल पेड़ पड़ता , जिसके नीचे गर्मी के दिन बीत...